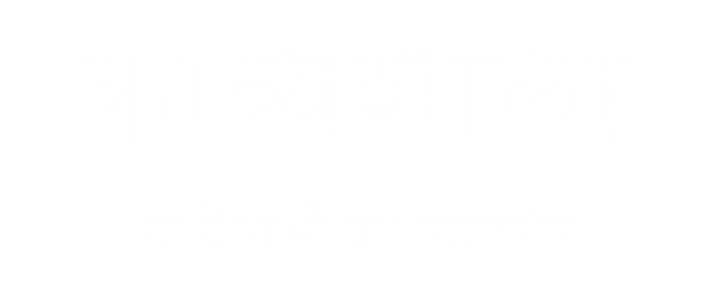ये जीत-हार तो इस दौर का मुक्द्दर है ये दौर जो के पुराना नही नया भी नहीं ये दौर जो सज़ा भी नही जज़ा भी नहीं ये दौर जिसका बा-जहिर कोइ खुदा भी नहीं तुम्हारी जीत अहम है ना मेरी हार अहम के इब्तिदा भी नहीं है ये इन्तेहा भी नहीं शुरु मारका-ए-जान अभी हुआ भी नहीं शुरु तो ये हंगाम-ए-फ़ैसला भी नहीं
Category: उर्दू शायरी
दायरा – कैफ़ि आज़मी
रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ बारहा तोड़ चुका हूँ जिन को इन्हीं दीवारों से टकराता हूँ रोज़ बसते हैं कई शहर नये रोज़ धरती में समा जाते हैं ज़लज़लों में थी ज़रा सी गिरह वो भी अब रोज़ ही आ जाते हैं
दस्तूर क्या ये शहरे-सितमगर – कैफ़ि आज़मी
दस्तूर[1] क्या ये शहरे-सितमगर[2] के हो गए । जो सर उठा के निकले थे बे सर के हो गए । ये शहर तो है आप का, आवाज़ किस की थी देखा जो मुड़ के हमने तो पत्थर के हो गए ।
तुम परेशां न हो – कैफ़ि आज़मी
तुम परेशां न हो बाब-ए-करम-वा न करो और कुछ देर पुकारूंगा चला जाऊंगा इसी कूचे में जहां चांद उगा करते थे शब-ए-तारीक गुज़ारूंगा चला जाऊंगा रास्ता भूल गया या यहां मंज़िल है मेरी कोई लाया है या ख़ुद आया हूं मालूम नहीं कहते हैं कि नज़रें भी हसीं होती हैं मैं भी कुछ लाया हूं क्या लाया मालूम नहीं
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो – कैफ़ि आज़मी
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या ग़म है जिस को छुपा रहे हो आँखों में नमी हँसी लबों पर क्या हाल है क्या दिखा रहे हो बन जायेंगे ज़हर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो
तुम – कैफ़ि आज़मी
शगुफ्तगी का लताफ़त का शाहकार हो तुम, फ़क़त बहार नहीं हासिल-ऐ-बहार हो तुम, जो इक फूल में है क़ैद वो गुलिस्तान हो, जो इक कली में है पिन्हाँ वो लाला-ज़ार हो तुम.
चरागाँ – कैफ़ि आज़मी
एक दो भी नहीं छब्बीस दिये एक इक करके जलाये मैंने इक दिया नाम का आज़ादी के उसने जलते हुये होठों से कहा चाहे जिस मुल्क से गेहूँ माँगो हाथ फैलाने की आज़ादी है
ज़िन्दगी – कैफ़ि आज़मी
आज अन्धेरा मिरी नस-नस में उतर जाएगा आँखें बुझ जाएँगी बुझ जाएँगे एहसास ओ शुऊर और ये सदियों से जलता-सा सुलगता-सा वजूद इस से पहले कि सहर माथे पे शबनम छिड़के इस से पहले कि मिरी बेटी के वो फूल से हाथ गर्म रुख़्सार को ठण्डक बख़्शें इस से पहले कि मिरे बेटे का मज़बूत बदन तन-ए-मफ़्लूज में शक्ति भर दे इस से पहले कि मिरी बीवी के होंट
कोई ये कैसे बताये – कैफ़ि आज़मी
कोई ये कैसे बता ये के वो तन्हा क्यों हैं वो जो अपना था वो ही और किसी का क्यों हैं यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों हैं यही होता हैं तो आखिर यही होता क्यों हैं एक ज़रा हाथ बढ़ा, दे तो पकड़ लें दामन उसके सीने में समा जाये हमारी धड़कन इतनी क़ुर्बत हैं तो फिर फ़ासला इतना क्यों हैं
काफ़िला तो चले – कैफ़ि आज़मी
ख़ारो-ख़स[1] तो उठें, रास्ता तो चले मैं अगर थक गया, काफ़िला तो चले चाँद-सूरज बुजुर्गों के नक़्शे-क़दम ख़ैर बुझने दो इनको, हवा तो चले हाकिमे-शहर, ये भी कोई शहर है मस्जिदें बन्द हैं, मयकदा तो चले